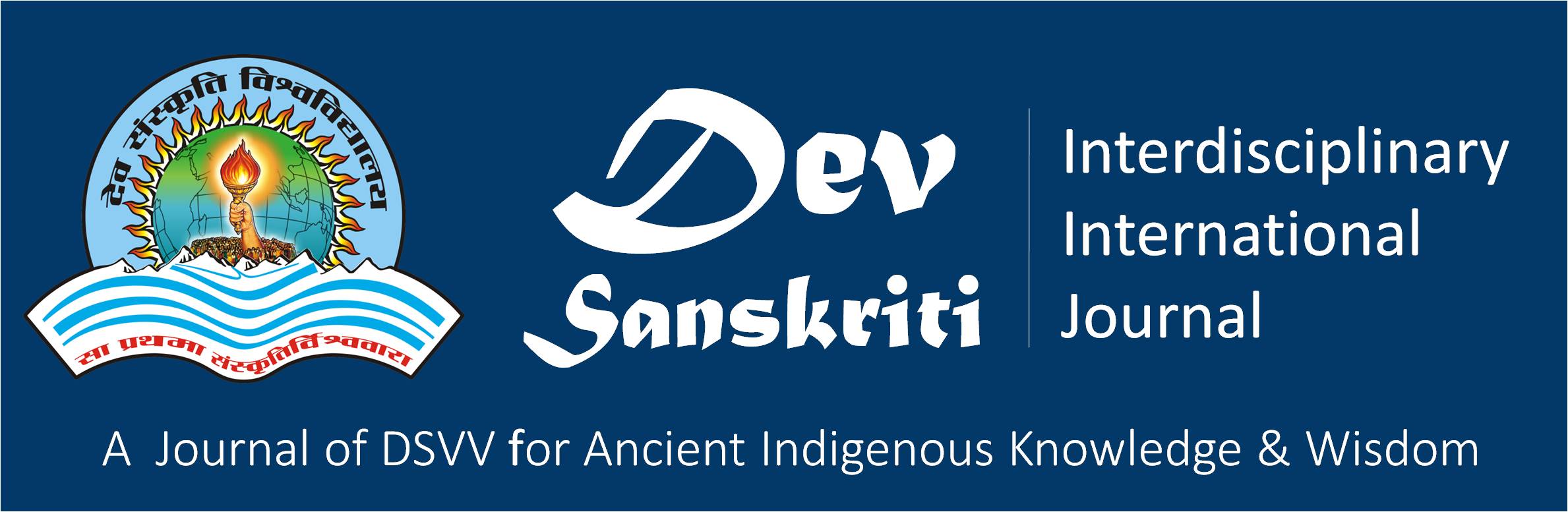Abstract
??????? ??? ??? ??????? ?? ???? ???????? ?????? ??? ??????? ?? ???? ???? ?????????? ?? ?????? ????? ???? ?????? ?? ???? ?????? ?? ???? ??? ???? ???? ??? ?????? ??? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ???? ?? ??????? ??? ??????? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????? ???? ?? ???-??? ?? ?????? ?? ?????????? ?Ÿ?? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ????????? ??? ?????Ÿ? ?? ?????? ??????? ?? ????? ?? ???? ?? ??????? ???? ???????? ?????? ?? ????? ??? ?????? ???? ?? ???????? ???? ?????? ???????? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ???? ???? ?? ?? ?????? ??????? ???? ?? ???? ??? ???? ?????????? ??? ??? ?????? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ?????? ????? ??? ??????? ?? ???? ?? ?? ??- ???? ?????? ?? ???? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ??? ??? ?????? ????? ??? ?????????? ?????? ?? ?? ????? ???? ??? ???????? ??? ????? ?? ?????? ?? ??????? ?? ???????? ????? ?????? ?? ???????? ??? ?? ??????? ??? ?? ???? ?? ?? ??????? ?? ???????? ?????? ?? ?????? ?? ????? ?? ????? ?? ??? ????? ????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ??? ???? ?? ?????????? ?? ???? ????? ??? ??? ???????? ?? ??????? ?? ??Ÿ? ?? ?? ???? ???? ??? ???????? ?? ??? ??????? ???? ????? ?? ?? ???????? ?? ?????? ????? ?????? ?? ???????? ????, ?? ?? ????? ?? ??????? ?????? ??? ?????-??????? ?? ???-??? ???????, ??????? ??? ?????? ?? ???? ?????? ????? ?? ????? ?? ????? ??? ???, ?? ????? ??? ?? ?? ???, ?????? ??? ?? ???? ????? ?? ????????? ?? ??? ??? ???? ????? ??? ?????? ?? ?????? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ? ????? ??? ?? ??Ÿ? ???? ??? ?? ???????? ???? ?????? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ????? ???? ?? ?? ???????? ???? ??????? ?? ??????????? ?? ???????? ???? ??? ????? ???? ?? ?? ???? ?????? ?? ?????? ?? ?? ???? ????? ?Ÿ??? ?? ????? ?? ?????? ??? ?? ????? ???? ??? ????? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ?? ???? ??? ????????? ????? ??? ????? ??? ????????? ???? ?? ???? ????? ????, ???????? ?? ?????? ?? ????? ???? ??? ????? ???????? ?? ?????? ??? ?? ???????? ?? ?????? ??? ??? ???? ?????????, ?????????? ?? ?????? ?? ??????? ??? ??????????? ?? ?????? ??????? ??????? ??? ???? ??????? ?? ??????? ???? ?? ??????? ?? ?????? ???? ?? ????? ????? ?????, ????? ?? ????????? ???? ??? ???? ??? ??? ????? ?? ???????? ?? ??? ?? ?????? ??? ?????? ?? ?????? ???? ???? ????? ?????? ?? ??? ?? ??? ????? ???? ????? ?? ????? ??????? ???? ???
References
Brahmavarchas (1998) Pt. Shriram Sharma Acharya Vangmay - विज्ञान और अध्यात्म परस्पर पूरक [Science And Spirituality Mutual Supplement], (Volume 23). Yug Nirman Yojana, Mathura, Page. 5.21.
Acharya Shriram Sarma (1967) व्यक्ति के मूल्यांकन का मापदण्ड बदल [Change the criteria for evaluating a person] Akhand Jyoti, Year 27, Issue 3, Page.13.
J. Arthur Thomson 1911 - Introduction to Science. H. Holt, New york city , p. 205. https://doi.org/10.1037/13760-000
Friedrich Max Muller 1977 The Six Systems Indian Philosophy, AMS Press California Vol. I, P. 24.
Brahmavarchas (1998) Pt. Shriram Sharma Acharya Vangmay - विज्ञान और अध्यात्म परस्पर पूरक [Science And Spirituality Mutual Supplement], (Volume 23). Yug Nirman Yojana, Mathura, Page. 5.23.
Brahmavarchas (1998) Pt. Shriram Sharma Acharya Vangmay - विज्ञान और अध्यात्म परस्पर पूरक [Science And Spirituality Mutual Supplement], (Volume 23). Yug Nirman Yojana, Mathura, Page. 5.21. P. 5.24.
Ranganathanand, Swami (1999). परिवर्तनशील समाज के लिए शाश्वत मूल्य [Charitable Values for A Transitional Society]. Ramkrishna Math, Nagpur. Page. 137
Vivekand S. 1962. The Complete works of Swami Vivekand, Vol. II P. 432. Advaita Ashram, Calcutta.
Swami Vivekananda (1989) Vivekananda Literature, Volume 3. Advaita Ashrama kolkata, Page. 119.
Dr. Radhakrishnan (1962). East And West Some reflection, DelhiRajpal and Sons, Page. 42
Mundakopanishad, 1/15, Max Muller (1962), The Upanishads - Part II, Dover Publications, ISBN 978-0486209937,
Goyandka, Jaya Dayal. (2014). Bhagavad Gita, 6.44, Geeta Press Gorakhpur.
Vivekand S. 1962. The Complete works of Swami Vivekand, Vol 1, PP.-Xiii-Xiv

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.